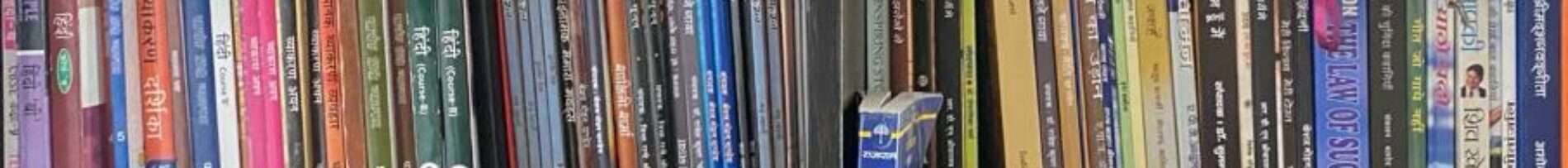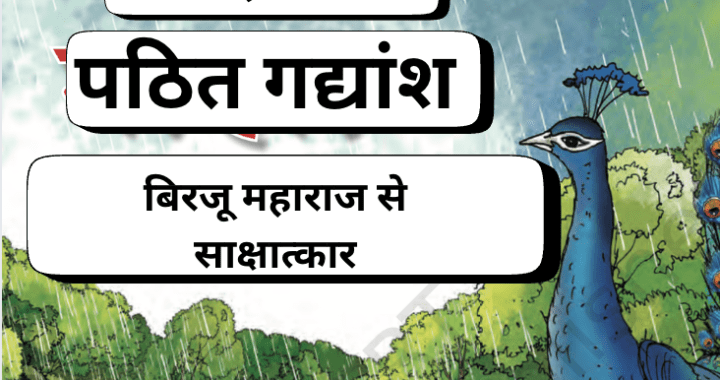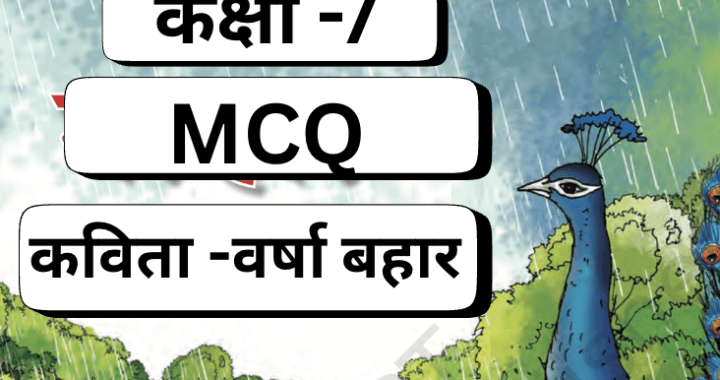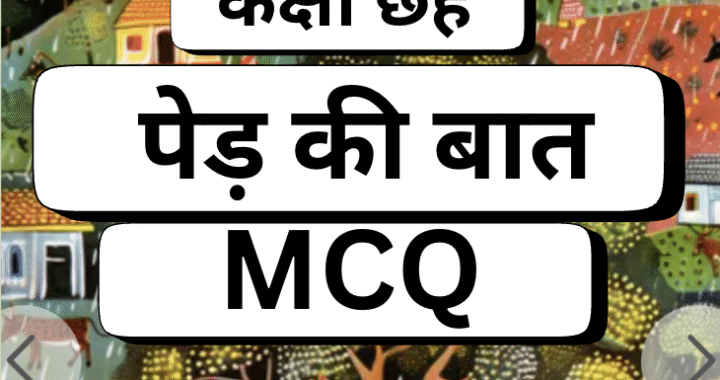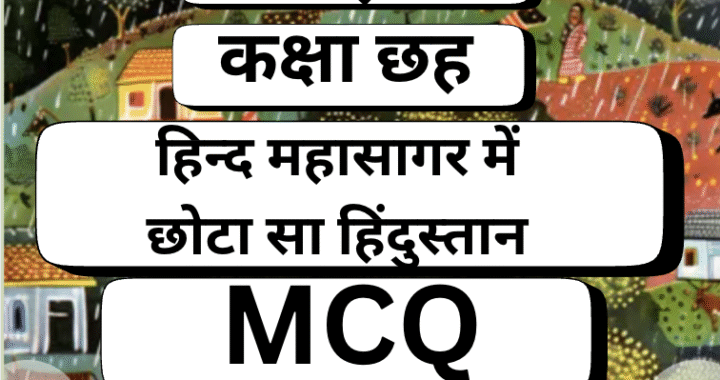संगीत की व्याख्या musical interpretation
1 min read
sangeet

You May Like –विडियो – वाराणसी
संगीत – संगीत एक कला है जिसमें ध्वनि, स्वर और लय का प्रयोग करके भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है।इसे स्वर और लय के प्रयोग से भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका माना जाता है। संगीत में गायन, वादन और नृत्य शामिल हो सकते हैं।
स्वर – स्वर शब्द का प्रयोग उस निश्चित ध्वनि या नोट के लिए किया जाता है जो संगीत में उपयोग की जाती है। यह संगीत की एक बुनियादी इकाई है संगीत में, स्वर एक निश्चित आवृत्ति वाली ध्वनि है जो संगीत की आधारशिला है। यह एक ऐसी पिच है जो संगीतकार द्वारा अपनी धुन और रागों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है स्वर एक निश्चित रूप, कोमलता या तीव्रता, और उतार–चढ़ाव का पता लगाने वाली ध्वनि है।
भारतीय संगीत में मुख्य रूप से सात स्वर होते हैं. ये हैं: षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिन्हें सामान्य रूप से सा, रे, गा, म, प, ध, नि कहा जाता है.
हालांकि, भारतीय संगीत में 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर शामिल हैं. विकृत स्वरों को कोमल (कम) और तीव्र (अधिक) के रूप में विभाजित किया जा सकता है.
सप्तक – संगीत में, सप्तक तीन प्रकार के होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, और तार सप्तक.
मंद सप्तक – यह मध्य सप्तक से एक सप्तक नीचे होता है और कम आवृत्ति वाले स्वरों को दर्शाता है। इन स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है।
मध्य सप्तक – यह मूल सप्तक है, जिसमें सात स्वर होते हैं।
तार सप्तक – यह मध्य सप्तक से एक सप्तक ऊपर होता है और उच्च आवृत्ति वाले स्वरों को दर्शाता है।इन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है।
You May Like – Calligraphy
लय – संगीत में लय, ध्वनियों और विश्राम की व्यवस्था से समय में बना एक पैटर्न है। इसे संगीत में गति और संरचना प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है
लय को आमतौर पर तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है-
विलंबित लय – यह धीमी गति की लय है, जो संगीत में धीमी और शांत भावना को व्यक्त करती है।
मध्यम लय – यह सामान्य गति की लय है, जो संगीत में सामान्य गति और संतुलन को दर्शाती है।
द्रुत लय – यह तेज गति की लय है, जो संगीत में ऊर्जा और गति को दर्शाती है।
थाट – थाट रागों को वर्गीकृत करने का एक बुनियादी तरीका है। इसे एक मूल पैमाना कहा जाता है जिसमें सात स्वर होते हैं। थाट को रागों की उत्पत्ति का आधार माना जाता है।
थाट के नियम: थाट में 12 स्वरों में से 7 स्वर होने चाहिए। थाट में आरोह या अवरोह (या दोनों) हो सकते हैं।थाट में एक ही स्वर के दो रूप (जैसे, कोमल नी और शुद्ध नी) नहीं हो सकते.
भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल 10 थाट होते हैं। इन थाटों से ही विभिन्न रागों की उत्पत्ति होती है –
इन 10 थाटों के नाम इस प्रकार हैं –
1.बिलावल 2.कल्याण
3.खमाज 4.भैरव
5.पूर्वी 6.मारवा
7.काफी 8.आसावरी
9.भैरवी 10.तोड़ी
आरोह –आरोह” का अर्थ है स्वरों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम में जाना या चढ़ना. जब संगीत में स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कि ‘स‘, ‘रे‘, ‘ग‘, ‘म‘, ‘प‘, ‘ध‘, ‘नि‘ क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे आरोह कहते हैं।
अवरोह – अवरोह का अर्थ है स्वरों का घटते क्रम में जाना, जैसे नि ध प म ग रे स। अवरोह में ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं
जाति – जाति किसी राग के स्वरों की संख्या और उनके आरोह (ऊपर की ओर) और अवरोह (नीचे की ओर) में प्रयोग को संदर्भित करता है।
वादी स्वर – वादी स्वर उस स्वर को कहा जाता है जो राग का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्वर होता है। इसे राग का राजा स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि राग में सबसे अधिक ठहराव इसी स्वर पर होता है और इसका बार–बार प्रयोग किया जाता है. यह स्वर राग की पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक है
संवादी स्वर – संवादी स्वर राग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, जो “वादी स्वर के बाद आता है। यह राग की पहचान को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भले ही वादी स्वर सबसे मुख्य स्वर हो।
स्थाई स्वर – यह वह स्वर होता है जो राग या गीत में बार–बार दोहराया जाता है, और यह राग की पहचान या गीत का मुख्य भाग होता है. इसे मुख्य स्वर भी कहते हैं.।
अंतरा – अंतरा का अर्थ है एक गीत के भीतर वह भाग जो मुखड़े (स्थायी) के बाद आता है, और यह एक अलग छंद होता है. इसे गाने के बीच का वह पैराग्राफ कहा जा सकता है जो मुखड़े से अलग होता है।
गायन समय – प्रत्येक राग के लिए निर्धारित समय, जो दिन या रात के विभिन्न प्रहरों (समय खंडों) से जुड़ा होता है. संगीत के नियमों के अनुसार, प्रत्येक राग को अपनी प्रकृति और विशेषताओं के अनुसार एक विशिष्ट समय पर गाया या बजाया जाता है और इसे ही गायन समय कहते हैं।
पकड़ – पकड़ वह छोटा सा स्वर समुदाय है जिसे गाने–बजाने से किसी राग विशेष का बोध हो जाए । उदाहरणार्थ– प रे ग रे, नि रे सा गाने से कल्याण राग का बोध होता है। यह संगीत से सम्बंधित लेख एक आधार है।
गत – विभिन्न प्रकार के वाद्यों पर बजायी जाने वाली ताल में बंधी हुई रचनाएँ गत कहकर पुकारी जाती हैं । संगीत में ‘गत‘ एक रचना या रूप है, जो विशेष रूप से ताल और वाद्य के बोलों के साथ निश्चित राग के स्वरों को बांधता है। यह मुख्य रूप से वाद्य संगीत में इस्तेमाल होता है, खासकर तबला और सितार में, और इसमें गीत के बोल नहीं होते हैं, बल्कि वाद्य के बोलों का उपयोग होता है.
गीत बंदिश – संगीत में गीत बंदिश एक विशिष्ट राग में निर्धारित, मधुर रचना है जो एक निश्चित ताल और लय में बंधी होती है. इसे एक विशिष्ट ताल (जैसे कि तीन ताल) में गाया या बजाया जाता है, और इसमें एक निश्चित स्वर–पद–ताल का समन्वय होता है।
लक्षण गीत – यह एक प्रकार का गीत होता है जो किसी राग के लक्षणों का वर्णन करता है। यह गीत राग के नाम, थाट, अनुवादी, विवादी, और प्रकृति जैसे लक्षणों को बताने में मदद करता है।
आलाप – संगीत में, आलाप (alap) राग के प्रदर्शन का पहला भाग होता है। यह राग की शुरुआत और उसके स्वरों की पहचान का एक प्रकार का मधुर सुधार होता है। आलाप में, संगीतकार धीरे–धीरे राग के स्वरों को उजागर करता है और राग की भावना को व्यक्त करता है ।आलाप राग के स्वरों, उसके मूड और प्रमुख स्वरों को प्रस्तुत करता है.
तान – यह एक एसी तकनीक है जिसमें स्वरों का उपयोग करके बहुत तेज़ और मधुर अंशों को सुधार किया जाता है. यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग के गायन में इस्तेमाल होती है
लय – संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं।लय” (Lay) को संगीत रचना में ध्वनियों और विश्राम के समय के एक निश्चित पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगीत को एक लयबद्ध संरचना प्रदान करता है और इसे जीवित बनाता है।
गीत में लय मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है– विलम्बित लय (धीमी गति), मध्य लय (मध्यम गति) और द्रुत लय (तेज़ गति). यह संगीत की गति और समय की अवधारणा से संबंधित है, जो संगीत की संरचना और अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है.
राग – संगीत में, राग एक विशिष्ट विधा है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अभिन्न अंग है। यह एक क्रमबद्ध स्वर–संग्रह है जो एक विशेष भावना या मूड को व्यक्त करता है। इसे एक “रंग” या “संवेदना” भी कहा जा सकता है जो संगीत सुनने वाले के मन पर प्रभाव डालता है. राग में उपयोग किए जाने वाले स्वरों का एक विशेष सेट होता है, जो आरोह और अवरोह (चढ़ना और उतरना) के नियमों के साथ होता है। हर राग की एक विशिष्ट ध्वनि होती है, जो कुछ विशेष भावनाओं, दिन के समय, और यहां तक कि मौसमों से जुड़ी होती है। राग में वादी (मुख्य स्वर), संवादी (द्वितीयक स्वर), और अनुवादी (अन्य स्वर) जैसे घटक शामिल होते हैं। प्रत्येक राग के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, जो बताते हैं कि स्वरों का कैसे उपयोग किया जाना चाहिए।
सम – यह ताल (rhythm) की पहली मात्रा को कहते हैं, जिस पर जोर दिया जाता है. यह ताल का आरंभ बिंदु होता है और इसे प्रायः ताली से चिह्नित किया जाता है.
ताल की सम मात्रा पर ही प्रायः गीत, गत, या नृत्य की शुरुआत होती है, और इसी मात्रा पर विशेष बल दिया जाता है.
दुगुन – संगीत में, दुगुन का अर्थ है एक मात्रा में दो बोलों का उच्चारण करना। इसका मतलब है कि एक बीट में दो मात्राएं होती हैं।
आवर्तन – संगीत में, आवर्तन (Aavartan) किसी ताल (ताल) का एक पूर्ण चक्र होता है, जो पहली मात्रा से शुरू होकर अंतिम मात्रा तक जाता है, फिर सम (Sam) पर वापस आता है. इसे ताल का एक आवृत्ति या चक्र भी कहा जाता है. आवर्तन ताल का एक पूरा चक्र है जो पहली मात्रा से शुरू होकर अंतिम मात्रा तक जाता है, फिर सम पर वापस आता है
नाद – नाद शब्द का अर्थ है कोई भी ध्वनि या कंपन जो सुनाई देती है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो संगीत के लिए आधारशिला है। नाद की विशेषता यह है कि यह एक विशिष्ट आवृत्ति वाली ध्वनि है जो कुछ समय तक बनी रहती है।
2,847 total views, 2 views today